सर्वोच्च न्यायालय की पूर्ण पीठ (Full Bench) ने विवादित वरिष्ठ अधिवक्ता श्री सिद्धार्थ लूथरा की अमाइकस क्यूरी (Amicus Curiae) के रूप में की गई नियुक्ति को समाप्त कर दिया तथा अटॉर्नी जनरल को न्यायालय की सहायता हेतु निर्देशित किया।
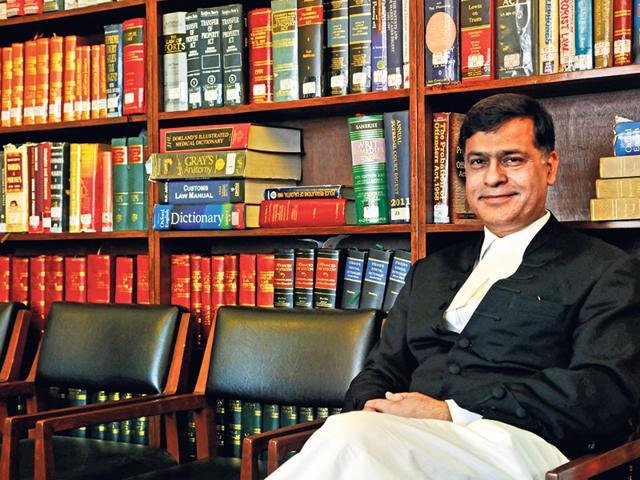
[Re: Vijay Kurle; प्रशांत भूषण बनाम भारत संघ, 2022 SCC OnLine SC 2222]
श्री लूथरा द्वारा न्यायालय के समक्ष अपनाए गए भ्रामक एवं कपटपूर्ण आचरण अनेक मामलों में उजागर हुए हैं। उन पर यह भी गंभीर आरोप है कि उन्होंने अधिवक्ताओं को फँसाने तथा उन्हें दंडित करवाने के उद्देश्य से न्यायालय को गुमराह किया और निरस्त (overruled) किए जा चुके निर्णयों का हवाला देकर न्यायालय से प्रतिकूल आदेश प्राप्त किए। उनके इन कपटपूर्ण तर्कों पर भरोसा करने वाले न्यायाधीशों की देशभर में व्यापक आलोचना हुई.
इसके अतिरिक्त, श्री लूथरा पर यह भी आरोप है कि उन्होंने एक अन्य मामले में अपनी मुवक्किल को अग्रिम ज़मानत दिलवाने के लिए सर्वोच्च न्यायालय के साथ धोखाधड़ी की तथा झूठे तथ्यों का प्रतिवेदन किया कि अन्य सह-अभियुक्तों को पहले ही ज़मानत मिल चुकी है। उक्त झूठी प्रस्तुति के आधार पर न्यायालय से ज़मानत आदेश प्राप्त किया गया। यह भी आरोप है कि उन्होंने न्यायाधीशों के नाम पर धनराशि स्वीकार की।
इस संबंध में गृह मंत्रालय, भारत सरकार ने उक्त शिकायत का संज्ञान लेते हुए बार काउंसिल को इस प्रकरण की विस्तृत जांच करने का निर्देश जारी किया है।
साथ ही, अधिवक्ता मिलिंद साठे, नितिन ठक्कर एवं अन्य के विरुद्ध भी कार्यवाही की मांग की गई है, जिन्होंने कथित रूप से इसी प्रकार के षड्यंत्रों में सम्मिलित होकर अनेक आपराधिक अपराधों एवं गंभीर पेशेवर दुराचार के कृत्य किए हैं। इन व्यक्तियों पर आरोप है कि उन्होंने ईमानदार अधिवक्ताओं के विरुद्ध झूठी और मनगढ़ंत शिकायतें तैयार कर प्रस्तुत कीं, जिनका उद्देश्य भ्रष्ट न्यायाधीशों को संरक्षण देना तथा न्यायिक जवाबदेही के हित में प्रारंभ की गई विधिक कार्यवाहियों को बाधित करना था।
मामले की संक्षिप्त पृष्ठभूमि (Brief Background of the Case):
अधिवक्ताओं के विरुद्ध प्रारंभ हुई ऐतिहासिक अवमानना (Contempt) कार्यवाही, Re: Vijay Kurle में, माननीय सर्वोच्च न्यायालय की पीठ, जिसकी अध्यक्षता माननीय न्यायमूर्ति दीपक गुप्ता कर रहे थे, ने अपने आदेश दिनांक 30.09.2019 द्वारा अधिवक्ता श्री सिद्धार्थ लूथरा को अमाइकस क्यूरी (Amicus Curiae) के रूप में नियुक्त किया।
सुनवाई के दौरान, अधिवक्ता सिद्धार्थ लूथरा ने श्री मिलिंद साठे द्वारा दायर शिकायत के समर्थन में पक्ष रखते हुए निम्नलिखित तर्क प्रस्तुत किए —
(i) उन्होंने न्यायालय को गुमराह करते हुए यह प्रतिवेदन किया कि Pritam Pal v. High Court of M.P., 1993 Supp (1) SCC 529, तथा C.K. Daphtary के पुराने मामले में दिया गया निर्णय बाध्यकारी (binding) है, और यह कि सर्वोच्च न्यायालय को अधिवक्ताओं या नागरिकों को अपनी इच्छा से दोषी ठहराने और दंडित करने की पूर्ण स्वतंत्रता प्राप्त है। उन्होंने यह भी कहा कि कोई भी कानून या संवैधानिक प्रावधान सर्वोच्च न्यायालय को सीमित नहीं कर सकता तथा न्यायालय किसी विधि या प्रक्रिया का पालन करने के लिए बाध्य नहीं है।
(ii) उन्होंने आगे यह तर्क दिया कि P.N. Duda v. P. Shiv Shanker, (1988) 3 SCC 167 में जो प्रक्रिया अवमानना का संज्ञान लेने हेतु निर्धारित की गई है, वह अनिवार्य (mandatory) नहीं है।
(iii) उन्होंने यह भी प्रतिवेदन किया कि यदि कोई न्यायाधीश भ्रष्टाचार में लिप्त हो या कोई गंभीर त्रुटि करे, तब भी किसी नागरिक या अधिवक्ता को ऐसे न्यायाधीश के विरुद्ध शिकायत करने का अधिकार नहीं है, और यह कि भले ही न्यायाधीश के विरुद्ध लगाए गए आरोप सत्य हों और ठोस प्रमाणों पर आधारित हों, न्यायालय उस व्यक्ति को केवल न्यायाधीशों के विरुद्ध बोलने के कारण दंडित कर सकता है।
उपर्युक्त सभी तर्क और प्रतिवेदन वस्तुतः माननीय सर्वोच्च न्यायालय की पूर्ण पीठ (Full Bench) एवं संविधान पीठों (Constitution Benches) द्वारा पहले ही स्पष्ट रूप से अस्वीकार (overruled) किए जा चुके हैं। इस विषय में निम्नलिखित निर्णय निर्णायक हैं —
- Bal Thackrey v. Harish Pimpalkhute, (2005) 1 SCC 254;
- Subramanian Swamy v. Arun Shourie, (2014) 12 SCC 344;
- Indirect Tax Practitioners’ Association v. R.K. Jain, (2010) 8 SCC 281;
- Hari Das v. State of West Bengal, (1964) 7 SCR 237।
उपर्युक्त संविधान पीठों एवं विस्तृत पीठों के निर्णयों में स्पष्ट रूप से निम्नलिखित विधिक सिद्धांत स्थापित किए गए हैं —
(i) P.N. Duda v. P. Shiv Shanker, (1988) 3 SCC 167 में दिए गए दिशा-निर्देश अनिवार्य एवं बाध्यकारी हैं, और उनका पालन न किए जाने से संपूर्ण अवमानना कार्यवाही अमान्य (vitiated) हो जाती है।
(ii) Pritam Pal v. High Court of M.P., 1993 Supp (1) SCC 529 का निर्णय स्पष्ट रूप से निरस्त (overruled) किया जा चुका है, और न्यायालयों पर यह वैधानिक दायित्व है कि वे Contempt of Courts Act, 1971 के अनिवार्य प्रावधानों का पालन करें।
(iii) जहाँ कहीं भी किसी न्यायाधीश के आचरण में दुर्व्यवहार (misconduct) अथवा भ्रष्टाचार (corruption) के ठोस प्रमाण मौजूद हों, वहाँ प्रत्येक नागरिक का यह संवैधानिक कर्तव्य (Constitutional Duty) है — जैसा कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 51-A में निर्दिष्ट है — तथा प्रत्येक अधिवक्ता का यह व्यावसायिक दायित्व (Professional Obligation) है — जैसा कि Bar Council of India Rules में विनिर्दिष्ट है — कि वह ऐसे दुराचार या भ्रष्टाचार को उजागर करे।
किसी भी चापलूस व्यक्ति या संगठन द्वारा सत्य के प्रकटीकरण (publication of truth) पर अवमानना कार्यवाही प्रारंभ करने का प्रयास किया जाना न केवल असंवैधानिक एवं विधि-विरुद्ध है, बल्कि ऐसे व्यक्ति या संस्था पर दृष्टांतात्मक क्षतिपूर्ति (exemplary costs) लगाई जा सकती है तथा उनके विरुद्ध भारतीय दंड संहिता की धारा 211 एवं 192 के अंतर्गत फौजदारी अभियोजन (criminal prosecution) भी चलाया जा सकता है।
परंतु, न्यायमूर्ति (सेवानिवृत्त) दीपक गुप्ता एवं अनिरुद्ध बोस की खंडपीठ ने अधिवक्ता श्री सिद्धार्थ लूथरा द्वारा प्रस्तुत तर्कों पर भरोसा करते हुए अपने निष्कर्ष निरस्त (overruled) किए जा चुके निर्णयों पर आधारित किए, तथा संविधान पीठों (Constitution Benches) के बाध्यकारी निर्णयों की पूर्णतः उपेक्षा करते हुए अधिवक्ताओं को दोषी ठहराया।
[Vijay Kurle, In Re, (2021) 13 SCC 616]
विस्तृत विवरण (Detailed Background):
परंतु, माननीय न्यायमूर्ति (सेवानिवृत्त) दीपक गुप्ता एवं माननीय न्यायमूर्ति अनिरुद्ध बोस की खंडपीठ ने अधिवक्ता श्री सिद्धार्थ लूथरा द्वारा प्रस्तुत तर्कों पर भरोसा करते हुए अपने निष्कर्ष निरस्त (overruled) किए जा चुके निर्णयों पर आधारित किए, तथा संविधान पीठों (Constitution Benches) के बाध्यकारी निर्णयों की पूर्णतः उपेक्षा करते हुए अधिवक्ताओं को दोषी ठहराया।
[Vijay Kurle, In Re, (2021) 13 SCC 616]
उक्त निर्णय के पश्चात्, संबंधित न्यायाधीशों के आचरण और उनके निर्णय को लेकर विधि समुदाय (legal fraternity) में तीव्र निंदा और आलोचना हुई। यह कहा गया कि उन्होंने विधि के मूलभूत सिद्धांतों की जानकारी न रखते हुए तथा लघु पीठों (smaller benches) के निरस्त निर्णयों के आधार पर अधिवक्ताओं को दंडित कर, अवमानना अधिकार (contempt jurisdiction) का दुरुपयोग किया।
प्रख्यात मानवाधिकार कार्यकर्ता एवं वरिष्ठ अधिवक्ता श्री असीम पंड्या, जो “Law of Contempt” विषय पर प्रसिद्ध ग्रंथ के लेखक हैं, ने LiveLaw पोर्टल पर दिनांक 16.09.2020 को एक विस्तृत आलेख प्रकाशित किया, जिसका शीर्षक था —
“Arrogation of Unlimited Contempt Power by the Supreme Court – A Hornets’ Nest Stirred Up Again.”
इस आलेख में श्री पंड्या ने उक्त निर्णय का गंभीर विश्लेषण करते हुए विस्तारपूर्वक यह स्पष्ट किया कि Re: Vijay Kurle तथा Re: Prashant Bhushan के निर्णय विधि की दृष्टि से त्रुटिपूर्ण (bad precedents) हैं, क्योंकि ये निर्णय पूर्व में निरस्त किए जा चुके तर्कों पर आधारित हैं तथा संविधान पीठों के बाध्यकारी निर्णयों के प्रतिकूल हैं।
आगे की कार्यवाही का विवरण (Subsequent Proceedings):
उक्त निर्णय को तत्पश्चात् अधिवक्ता प्रशांत भूषण, अधिवक्ता निलेश ओझा, अधिवक्ता विजय कुरले, तथा राशिद खान पठान द्वारा माननीय सर्वोच्च न्यायालय में दायर विभिन्न रिट याचिकाओं के माध्यम से चुनौती दी गई। ये याचिकाएँ दिनांक 17.05.2022 को सर्वोच्च न्यायालय की तीन-सदस्यीय पीठ (Three-Judge Bench) के समक्ष सुनवाई हेतु सूचीबद्ध थीं।
उस दिन, वरिष्ठ अधिवक्ता राजीव धवन, अधिवक्ता निलेश ओझा, अधिवक्ता पार्थो सरकार, अधिवक्ता विजय कुरले, अधिवक्ता तनवीर निज़ाम, अधिवक्ता आनंद जोंधले,अँड. ईश्वरलाल अग्रवाल तथा लगभग 200 अन्य अधिवक्ता, सर्वोच्च न्यायालय में उपस्थित हुए और याचिकाकर्ताओं के समर्थन में प्रस्तुत हुए।
सुनवाई के दौरान, अधिवक्ता सिद्धार्थ लूथरा, जिन्होंने पूर्व में अधिवक्ताओं के विरुद्ध पक्ष रखा था, स्वतः (on his own) न्यायालय के समक्ष उपस्थित हुए और यह दावा करते हुए प्रस्तुति देने का प्रयास किया कि वे अभी भी Amicus Curiae के रूप में कार्यरत हैं।
परंतु माननीय भारत के मुख्य न्यायाधीश (Chief Justice of India) ने उन्हें सुनने से इंकार कर दिया और यह टिप्पणी की कि उनका Amicus Curiae के रूप में कार्यकाल Re: Vijay Kurle मामले के निर्णय के साथ ही समाप्त हो चुका है। न्यायालय ने निर्देश दिया कि अब से भारत के अटॉर्नी जनरल इस मामले में न्यायालय की सहायता करेंगे।
सैकड़ों अधिवक्ताओं के समक्ष हुई इस फटकार और अपमान के पश्चात्, तथा यह समझते हुए कि उनके अनुचित आचरण का पर्दाफाश हो चुका है, अधिवक्ता सिद्धार्थ लूथरा न्यायालय कक्ष से बाहर चले गए।
इसके बाद, पूर्ण पीठ (Full Bench) ने उपरोक्त रिट याचिकाओं को स्वीकार करते हुए याचिकाकर्ताओं को अंतरिम राहत (interim relief) प्रदान की तथा उनके विरुद्ध दी गई सजा पर रोक (stay on sentence) लगा दी।
[Prashant Bhushan v. Union of India, 2022 SCC OnLine SC 2222]
बाद में, अधिवक्ता सिद्धार्थ लूथरा ने इस मामले में फिर कभी भी उपस्थित होने का साहस नहीं किया। उनकी बेईमानी और भ्रष्ट आचरण उस समय तक पूर्णतः उजागर और सिद्ध हो चुके थे।
Re: Vijay Kurle निर्णय की विधिक स्थिति (Legal Status of the Judgment in Re: Vijay Kurle):
Re: Vijay Kurle का निर्णय एक “Per Incuriam and Non-Binding Precedent” (कानून के विपरीत एवं विधिक सिद्धांतों की अनदेखी में पारित तथा बाध्यकारी न रहने वाला निर्णय) है, क्योंकि यह निर्णय Pritam Pal v. High Court of M.P., 1993 Supp (1) SCC 529 जैसे निरस्त (Overruled) किए जा चुके निर्णय पर आधारित था।
इसके अतिरिक्त, C.K. Daphtary v. O.P. Gupta, (1971) 1 SCC 626 का निर्णय भी वैधानिक (Statutorily) तथा निहित रूप से (Impliedly) निरस्त एवं अप्रभावी (Overruled and No Longer Binding) घोषित किया गया है, जैसा कि P.N. Duda v. P. Shiv Shanker, (1988) 3 SCC 167 (para 39) तथा Biman Basu v. Kallol Guha Thakurta, (2010) 8 SCC 673 (para 23) में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा स्पष्ट किया गया है।
साथ ही, C.K. Daphtary v. O.P. Gupta, (1971) 1 SCC 626 का निर्णय स्वयं में भी “Per Incuriam” है, क्योंकि यह संविधान पीठ (Constitution Bench) के निर्णय Bathina Ramakrishna Reddy v. State of Madras, 1952 SCR 425 के विपरीत है।
Bathina Ramakrishna Reddy के मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने स्पष्ट रूप से यह सिद्धांत प्रतिपादित किया कि —
“यदि किसी न्यायाधीश के भ्रष्टाचार या दुराचार के ठोस प्रमाण उपलब्ध हों, तो ऐसे तथ्यों को सार्वजनिक रूप से उजागर करना जनता के हित में एक वैध कर्तव्य है, और उसे न्यायालय की अवमानना नहीं कहा जा सकता। केवल झूठे या दुर्भावनापूर्ण आरोपों के मामलों में ही कार्रवाई की जा सकती है।”
इसी सिद्धांत को आगे बढ़ाते हुए संविधान पीठ ने Subramanian Swamy v. Arun Shourie, (2014) 12 SCC 344, तथा Indirect Tax Practitioners’ Association v. R.K. Jain, (2010) 8 SCC 281 के निर्णयों में भी यह स्पष्ट विधिक सिद्धांत (Legal Principle) स्थापित किया है कि —
“न्यायपालिका में व्याप्त भ्रष्टाचार को उजागर करना न केवल नागरिकों और अधिवक्ताओं का मौलिक अधिकार (Fundamental Right) है, बल्कि यह भारत के संविधान के अनुच्छेद 51-A के अंतर्गत प्रत्येक नागरिक का संवैधानिक कर्तव्य (Constitutional Duty) भी है।
सत्य तथ्यों का प्रकटीकरण (Disclosure of Truth) अथवा न्यायिक भ्रष्टाचार का पर्दाफाश न्यायालय की अवमानना नहीं माना जा सकता।”
अतः Re: Vijay Kurle का निर्णय न केवल Per Incuriam है, बल्कि यह संविधान पीठों के बाध्यकारी निर्णयों के प्रतिकूल होने के कारण विधिक रूप से अप्रभावी (Non-Est in Law) भी है।
विधिक परिणाम (Legal Consequences):
उपरोक्त तथ्यों एवं न्यायिक निर्णयों के परिप्रेक्ष्य में यह निर्विवाद रूप से स्थापित होता है कि Re: Vijay Kurle का निर्णय न केवल “Per Incuriam and Non-Binding Precedent” है, बल्कि यह संविधान पीठों (Constitution Benches) के बाध्यकारी निर्णयों के प्रतिकूल (Contrary to Binding Precedents) होने के कारण विधिक दृष्टि से शून्य (Void ab initio) और अप्रभावी (Non-Est in Law) है।
अतः इस निर्णय के आधार पर पारित कोई भी आदेश, दंडादेश या न्यायिक निष्कर्ष कानूनी वैधता नहीं रखता, और ऐसे सभी आदेश असंवैधानिक (Unconstitutional) एवं अमान्य (Invalid) माने जाएंगे।
परिणामस्वरूप —
1. Re: Vijay Kurle के निर्णय के आधार पर पारित किसी भी सजा या आदेश को स्वतः निरस्त (Automatically Set Aside) किया जाना आवश्यक है।
2. संबंधित न्यायाधीशों द्वारा निरस्त निर्णयों का अनुसरण करना और संविधान पीठों के आदेशों की उपेक्षा करना विधिक अनुशासन (Judicial Discipline) का गंभीर उल्लंघन है।
3. ऐसे आदेशों से प्रभावित अधिवक्ताओं एवं नागरिकों को संवैधानिक उपचार (Constitutional Remedies) एवं प्रतिपूरक क्षतिपूर्ति (Compensatory Relief) का अधिकार प्राप्त है।
4. इसके अतिरिक्त, न्यायालय को गुमराह करने वाले अधिवक्ताओं, विशेषतः अधिवक्ता सिद्धार्थ लूथरा, के विरुद्ध धारा 191, 192, 211 भारतीय दंड संहिता, तथा धारा 35, अधिवक्ता अधिनियम, 1961 के अंतर्गत फौजदारी एवं अनुशासनात्मक कार्यवाही (Criminal and Disciplinary Proceedings) प्रारंभ की जानी चाहिए।
अधिवक्ता श्री सिद्धार्थ लूथरा का अन्य प्रकरण में कदाचार एवं भ्रष्ट आचरण
(Gross Criminal and Professional Misconduct in Another Matter)
एक अन्य प्रकरण में, अधिवक्ता श्री सिद्धार्थ लूथरा पर यह गंभीर आरोप लगाया गया है कि उन्होंने अपनी मुवक्किल सुश्री गीता शेजवल की ओर से माननीय सर्वोच्च न्यायालय में अग्रिम जमानत (Anticipatory Bail) के आवेदन की सुनवाई के दौरान कपटपूर्ण आचरण (Fraud upon the Court) किया।
यह आरोप है कि श्री लूथरा ने न्यायालय के समक्ष झूठे और भ्रामक प्रतिवेदन प्रस्तुत करते हुए यह कहा कि सभी सह-अभियुक्तों को पहले ही अग्रिम जमानत प्रदान की जा चुकी है।
उक्त भ्रामक प्रस्तुति पर भरोसा करते हुए माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने उनकी मुवक्किल को अग्रिम जमानत प्रदान कर दी।
बाद में यह तथ्य सामने आया कि वास्तव में किसी भी सह-अभियुक्त को अग्रिम जमानत प्रदान नहीं की गई थी।
यह आचरण न केवल गंभीर आपराधिक कदाचार (Gross Criminal Misconduct) है, बल्कि यह व्यावसायिक नैतिकता (Professional Ethics) तथा अधिवक्ता अधिनियम, 1961 के प्रावधानों का भी घोर उल्लंघन है। उक्त कार्यवाही में उन्होंने न्यायालय के समक्ष जानबूझकर भ्रामक प्रतिवेदन (False and Misleading Representations) प्रस्तुत किए, जिससे न्यायालय को त्रुटिपूर्ण आदेश (Erroneous Order) पारित करने के लिए प्रेरित किया गया।
इसके पश्चात् एक विस्तृत शिकायत दायर की गई, जिसमें अधिवक्ता सिद्धार्थ लूथरा के विरुद्ध झूठी गवाही (Perjury) का अभियोजन प्रारंभ करने तथा गंभीर व्यावसायिक दुराचार (Gross Professional Misconduct) और न्यायालय की प्रक्रिया के दुरुपयोग (Abuse of Process of Court) के लिए अनुशासनात्मक कार्यवाही (Disciplinary Proceedings) आरंभ करने की मांग की गई।
उक्त शिकायत में यह भी आरोप लगाया गया है कि अधिवक्ता सिद्धार्थ लूथरा ने माननीय सर्वोच्च न्यायालय के कुछ न्यायाधीशों के नाम पर ₹10 करोड़ रुपये की राशि स्वीकार की।
इस गंभीर शिकायत पर गृह मंत्रालय, भारत सरकार ने संज्ञान (Cognizance) लिया है तथा इसे बार काउंसिल ऑफ इंडिया एवं संबंधित राज्य बार काउंसिल को आवश्यक अनुशासनात्मक एवं दंडात्मक कार्यवाही (Disciplinary and Penal Action) हेतु प्रेषित किया है।



