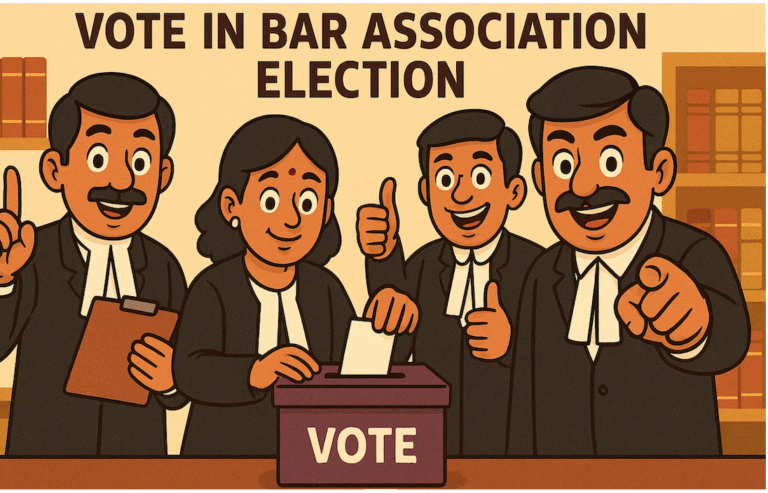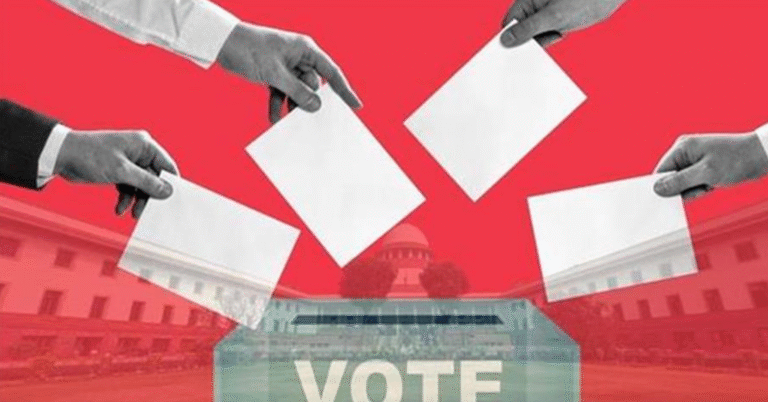अनुसूचित जाति/जनजाति और पिछड़े वर्ग समुदाय की महिला वकीलों सहित पंद्रह अधिवक्ताओं ने, मा. मुख्य न्यायाधीश चंद्रशेखर की अध्यक्षता वाले खंडपीठ द्वारा पारित आदेश से उनके मौलिक संवैधानिक अधिकारों का उल्लंघन होने का आरोप लगाते हुए, प्रत्येक को 50 लाख रुपये क्षतिपूर्ति दिलाने की मांग के साथ महाराष्ट्र राज्य के खिलाफ उच्च न्यायालय में पंद्रह याचिका दायर.

इससे पहले इसी प्रकार की गलती मुंबई उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति ज़ेड. ए. हक द्वारा की गई थी। उस समय मा. भारत के मुख्य न्यायाधीश श्री भूषण गवई की अध्यक्षता वाले खंडपीठ ने Suo Motu (Court on its Own Motion) v. T.G. Babul, 2018 SCC OnLine Bom 4853 मामले में उस अवैध अवमान कार्यवाही को रद्द ठहराया था तथा 16 अधिवक्ताओं से उच्च न्यायालय की ओर से माफी मांगते हुए खेद व्यक्त किया था।
लगभग 1,500 अधिवक्ताओं ने इन याचिकाकर्ताओं का प्रतिनिधित्व करने की तैयारी जताई है और उन्होंने Indian Bar Association कार्यालय में वकालतनामे प्रस्तुत किए हैं। इस मामले को वकालत की स्वतंत्रता (Independence of Bar) के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण मामला माना जा रहा है।
सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय ने अनेक मामलों में, विशेषकर Ramesh Maharaj v. Attorney General of Trinidad & Tobago, (1978) 2 WLR 902; Bharat Devdan Salvi v. State of Maharashtra, 2016 SCC OnLine Bom 42; तथा Walmik Bobde v. State of Maharashtra, 2001 ALL MR (Cri) 1731 में स्पष्ट रूप से यह विधिक सिद्धांत स्थापित किया है कि यदि न्यायालयीन आदेशों के कारण अधिवक्ताओं अथवा नागरिकों के किसी भी मौलिक अधिकारों का हनन होता है — जिसमें बिना आरोप तय किए और बिना न्यायिक प्रक्रिया का पालन किए दी गई अवमान दोषसिद्धि भी सम्मिलित है — तो ऐसे मामलों में राज्य क्षतिपूर्ति देने के लिए बाध्य होगा।
इससे पूर्व भी न्यायालयों ने गलत न्यायिक आदेशों और मूलभूत अधिकारों के उल्लंघन के मामलों में ₹25,000 से लेकर ₹5 करोड़ तक की क्षतिपूर्ति (मुआवज़ा) प्रदान की है
· Sarvepalli Radhakrishnan University v. Union of India, (2019) 14 SCC 761 – 5 करोड़ रुपये क्षतिपूर्ति।
· S. Nambi Narayanan v. Siby Mathews, (2018) 10 SCC 804 – 50 लाख रुपये क्षतिपूर्ति।
· Bharat Devdan Salvi v. State of Maharashtra, 2016 SCC OnLine Bom 42 – न्यायालयीन गलत आदेश के कारण क्षतिपूर्ति।
· Walmik Bobde v. State of Maharashtra, 2001 ALL MR (Cri) 1731 – न्यायालयीन गलत आदेश के कारण क्षतिपूर्ति।
इस प्रकरण में संबंधित अधिवक्ताओं को लेखी याचिका के माध्यम से क्षतिपूर्ति प्रदान की गई थी। न्यायालयों ने स्पष्ट रूप से कहा कि न्यायपालिका राज्य का अभिन्न अंग है और यदि किसी भी नागरिक के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होता है तो वह इस जिम्मेदारी से मुक्त नहीं हो सकती।
याचिका दायर करने वाले अधिवक्ता
इस याचिका को दायर करने वाले अधिवक्ताओं में शामिल हैं :
श्री विजय कुरले, श्री ईश्वरलाल अग्रवाल, श्री पार्थो सरकार, श्री अभिषेक एन. मिश्रा, कुमारी अनुश्का सोनवणे, श्री देवकृष्ण भांबरी, श्री शिवम गुप्ता, श्री विकास पवार, कुमारी निक्की पोकर, सौ. मीना ठाकुर, कुमारी प्रियांका शर्मा, कुमारी सोनल मांजरेकर, श्री सागर उगले, कुमारी निकिता किंजारा और श्री जयेंद्र मांजरेकर।
व्यावसायिक कदाचार पर कार्रवाई का अधिकार केवल बार काउंसिल को
अधिवक्ताओं पर “व्यावसायिक कदाचार” (Professional Misconduct) का ठपका लगाना या उन्हें चेतावनी (Warning) अथवा (Reprimand) जैसी सज़ा देना, यह अधिकार उच्च न्यायालय के पास नहीं है।
यह विधिक सिद्धांत सर्वोच्च न्यायालय की संविधान पीठ ने Supreme Court Bar Association v. Union of India, (1998) 4 SCC 409 प्रकरण में ठोस रूप से स्थापित किया है।
यह अधिकार केवल बार काउंसिल की अनुशासन समितियों (Disciplinary Committees of Bar Councils) को है। अधिवक्ताओं के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई करते समय इन समितियों के लिए यह अनिवार्य है कि वे फौजदारी मुकदमों की प्रक्रिया के अनुरूप कठोर नियमों का पालन करें, जैसा कि सर्वोच्च न्यायालय ने An Advocate v. Bar Council of India, 1989 Supp (2) SCC 25 प्रकरण में स्पष्ट रूप से रेखांकित किया है।
परंतु, इन ठोस कानूनी सीमाओं का उल्लंघन करते हुए, मुंबई उच्च न्यायालय की पाँच सदस्यीय खंडपीठ ने अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर जाकर 15 अधिवक्ताओं के विरुद्ध अवैध रूप से टिप्पणियाँ दर्ज कीं और उनके मौलिक अधिकारों का गंभीर हनन किया।
इसी कारणवश, क्षतिपूर्ति प्राप्त करने के लिए इन पंद्रह अधिवक्ताओं ने लेखी याचिका दायर की है।
याचिकाकर्ता अधिवक्ता एवं अधिवक्ता संघटनाओं का कहना है कि सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ द्वारा निर्धारित कानून — Subramanian Swamy v. Arun Shourie, (2014) 12 SCC 344 तथा Indirect Tax Practitioners’ Assn. v. R.K. Jain, (2010) 8 SCC 281 — के तहत इस प्रकरण में अधिवक्ताओं द्वारा की गई कार्यवाही केवल उनका संवैधानिक कर्तव्य (Constitutional Duty) थी। सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट रूप से यह कानून प्रतिपादित किया है कि न्यायाधीशों के भ्रष्टाचार को उजागर करना तथा उनके अपराधों पर कार्यवाही की मांग करना भारतीय संविधान के अनुच्छेद 51-अ के अंतर्गत प्रत्येक नागरिक और प्रत्येक अधिवक्ता का कर्तव्य है। और उन्हें अवमान कानून (Contempt Jurisdiction) का सहारा लेकर चुप नहीं कराया जा सकता।
तथा बार काउंसिल ऑफ इंडिया के नियमों के अनुसार प्रत्येक अधिवक्ता को, न्यायिक प्रणाली में व्याप्त भ्रष्टाचार, कदाचार अथवा न्यायाधीशों द्वारा किए गए गंभीर गैरवर्तन के विरुद्ध आवाज उठाना एवं उसे सार्वजनिक करना एक नैतिक तथा वैधानिक दायित्व है।
अतः अधिवक्ताओं द्वारा किया गया प्रकटीकरण और दिए गए वक्तव्य संवैधानिक तथा नैतिक कर्तव्य की परिधि में आते हैं; परिणामस्वरूप उन्हें अवमान नहीं ठहराया जा सकता।”**
मुंबई/दिल्ली :
एक महत्वपूर्ण और स्वागत योग्य घटनाक्रम के रूप में, पंद्रह अधिवक्ताओं ने — जिनमें अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और पिछड़े वर्ग समुदाय की महिला वकीलें भी शामिल हैं — महाराष्ट्र राज्य के विरुद्ध प्रति व्यक्ति 50 लाख रुपये की अंतरिम क्षतिपूर्ति की मांग को लेकर माननीय मुंबई उच्च न्यायालय में लेखी याचिका दाखिल की है।
याचिकाकर्ताओं का ठोस दावा है कि मा. मुख्य न्यायाधीश चंद्रशेखर की अध्यक्षता वाली पाँच न्यायमूर्तियों की खंडपीठ ने उनके मौलिक अधिकारों का गंभीर उल्लंघन किया है और इस कारण हुई अपरिमित हानि के लिए राज्य सरकार क्षतिपूर्ति देने के लिए बाध्य है।
याचिका में लगाए गए आरोप
याचिका में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि मौलिक अधिकारों का गंभीर और प्रत्यक्ष उल्लंघन निम्न प्रकार से हुआ:
· अधिवक्ताओं के विरुद्ध कठोर और प्रतिकूल टिप्पणियाँ (adverse strictures) की गईं,
· उन्हें अवमान और व्यावसायिक कदाचार के आरोप में दोषी ठहराया गया,
· यह सब बिना कोई नोटिस जारी किए, उन्हें पक्षकार बनाए बिना तथा उन्हें जवाब देने या पक्ष रखने का अवसर दिए बिना किया गया,
· समान परिस्थिति में खड़े अधिवक्ताओं के बीच भेदभाव किया गया — जहाँ एडवोकेट निलेश ओझा को आरोप तय करने से पूर्व जवाब दाखिल करने का अवसर दिया गया, वहीं अन्य 15 अधिवक्ताओं को यह अवसर न देकर सीधे चेतावनी के रूप में दंडित कर दिया गया।
‘न्यायिक प्रक्रिया के बिना अवमान का दोषारोप कर किसी को दोषी ठहराना असंभव’ : सुप्रीम कोर्ट की कड़ी चेतावनी
अवमानना (Contempt) प्रकरण में आरोपी को न्यायिक प्रक्रिया पूरी होने तक निर्दोष माने जाने का संवैधानिक अधिकार है। सुप्रीम कोर्ट ने यह स्पष्ट संदेश दिया है कि यदि कानून द्वारा निर्धारित प्रक्रिया का पालन न किया जाए, तो कोई भी न्यायालय सीधे किसी को दोषी नहीं ठहरा सकता।
न्यायालय ने स्पष्ट किया है कि अवमान कार्यवाही का स्वरूप अर्ध-फौजदारी (Quasi-Criminal) है। इसलिए इसे आपराधिक न्यायशास्त्र के सभी नियमों तथा प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों के अनुरूप ही चलाया जाना चाहिए।
आवश्यक प्रक्रिया के चरण
सुप्रीम कोर्ट के आदेशानुसार अवमान प्रकरण में दोषारोप (चार्ज) दर्ज करने के लिए निम्नलिखित चरण अनिवार्य हैं :
- सटीक आरोपों सहित स्पष्ट कारण बताओ नोटिस जारी करना,
- ठोस दोषारोप (चार्ज) तय करना,
- आरोपी को उत्तर देने और अपना बचाव प्रस्तुत करने का अवसर देना,
- मौखिक और दस्तावेजी सबूत प्रस्तुत करने तथा विरोधी पक्ष के गवाहों की जिरह (Cross-Examination) का अधिकार देना,
- पूर्ण और न्यायपूर्ण सुनवाई करना,
- और अंततः, आपराधिक मुकदमों की तरह “संदेह से परे प्रमाण” (Proof Beyond Reasonable Doubt) के सिद्धांत का पालन करना।
नियमों का उल्लंघन कर दोषारोप संभव नहीं
इन सभी प्रक्रियाओं के बिना किसी भी व्यक्ति या अधिवक्ता को अवमान प्रकरण में दोषी नहीं ठहराया जा सकता। किंतु यदि किसी न्यायालय ने इन नियमों का उल्लंघन कर अवैध आदेश पारित किया हो, तो उससे हुई क्षति की भरपाई करना राज्य सरकार की बाध्यता है।
सुप्रीम कोर्ट के संदर्भित निर्णय
इस संदर्भ में सुप्रीम कोर्ट ने अनेक प्रकरणों में स्पष्ट भूमिका रखी है, जिनमें शामिल हैं :
- L.P. Misra v. State of U.P. (1998)
- R.S. Sehrawat v. Rajeev Malhotra (2018)
- P. Mohanraj v. Shah Brothers Ispat Pvt. Ltd. (2021)
- Mehmood Pracha v. CAT (2022)
- Khushi Ram v. Sheo Vati (1953)
- S. Tirupathi Rao v. M. Lingamaiah (2024)
- R.S. Sujatha v. State of Karnataka (2011)
“समानता, न्यायप्रक्रिया और निष्पक्षता के सिद्धांतों पर प्रहार”
याचिकाकर्ताओं का ठोस आरोप है कि उच्च न्यायालय की खंडपीठ द्वारा की गई कार्यवाहियों ने भारतीय संविधान के मूलभूत स्तंभों — समानता (Equality), न्यायसंगत प्रक्रिया (Due Process) और निष्पक्षता (Fairness) — पर सीधा आघात किया है। ये मूल्य संविधान के अनुच्छेद 14, 19, 20 और 21 में स्पष्ट रूप से संरक्षित हैं।
कोई नोटिस दिए बिना, आरोप (Charges) तय किए बिना और सुनवाई का अवसर प्रदान किए बिना याचिकाकर्ताओं को अवमान और व्यावसायिक दुराचरण में दोषी ठहराकर दंडित करना न केवल उनके मूलभूत अधिकारों का उल्लंघन है, बल्कि याचिका में यह भी कहा गया है कि यदि इस प्रकार के आदेश कायम रहे, तो जनता का न्यायपालिका पर से विश्वास डगमगा जाएगा।
याचिकाकर्ताओं का यह भी कहना है कि क्षतिपूर्ति (Compensation) दया या कृपा की वस्तु नहीं है, बल्कि नागरिकों को हुई गंभीर क्षति के प्रति एक प्रवर्तनीय (enforceable) संवैधानिक अधिकार है।
जिम्मेदारी
याचिकाकर्ताओं का कहना है कि क्षतिपूर्ति प्रदान करना राज्य की कृपा या दानशीलता का विषय नहीं, बल्कि यह सर्वोच्च न्यायालय द्वारा विकसित किए गए बंधनकारी संवैधानिक सिद्धांतों से उत्पन्न संवैधानिक जिम्मेदारी है।
ऐसे मामलों में क्षतिपूर्ति का द्वि-आयामी उद्देश्य है —
1. पीड़ितों को न्यायालयीन अतिरेक (Judicial Excess) से हुई हानि के लिए कुछ राहत मिलना, और
2. यह प्रदर्शित करके जनता का न्यायपालिका पर विश्वास पुनः स्थापित करना कि न्यायपालिका भी संवैधानिक अनुशासन की सीमाओं से परे नहीं है।
जवाबदेही और दंड की मांग
भविष्य में ऐसे उल्लंघनों पर रोक लगाने हेतु कुछ अधिवक्ताओं ने दोषी न्यायाधीशों के विरुद्ध फौजदारी (Criminal) और दीवानी (Civil) कार्यवाही की अनुमति माँगते हुए आवेदन भी दायर किए हैं।
इसके लिए भारतीय दंड संहिता (IPC) की निम्नलिखित धाराओं का सहारा लिया गया है (और इनके समकक्ष भारतीय न्याय संहिता, 2023 की धाराएँ) :
- धारा 166 – जानबूझकर कानून का उल्लंघन करने वाले लोकसेवक,
- धारा 167 – गलत अथवा अवैध अभिलेख (रिकॉर्ड) तैयार करना,
- धारा 219 – अवैध न्यायनिर्णय देना,
- धारा 220 – किसी व्यक्ति को अवैध रूप से कैद करना अथवा मुकदमा चलाना,
- धारा 120-बी – आपराधिक षड्यंत्र (Criminal Conspiracy) रचना,
- धारा 34 और 107 – अवैध कृत्यों में सहभागिता या प्रोत्साहन देना।
साथ ही, nemo judex in causa sua (कोई भी व्यक्ति अपने ही मामले में न्यायाधीश नहीं हो सकता) के सिद्धांत का हवाला देते हुए इस मामले के लिए विशेष खंडपीठ गठित करने की भी मांग की गई है, ताकि यह सुनिश्चित हो कि —
“न्याय केवल किया ही न जाए, बल्कि न्याय होते हुए दिखाई भी दे।”
नुकसानभरपाई न्यायाधीशों से ही वसूल की जाए : सर्वोच्च न्यायालय का सिद्धांत
राज्य सरकार क्षतिपूर्ति (नुकसानभरपाई) देने के लिए बाध्य है ही; परंतु सुप्रीम कोर्ट ने यह ठोस कानून स्थापित किया है कि भरी गई क्षतिपूर्ति की राशि संबंधित गलत आदेश पारित करने वाले न्यायाधीशों और जिम्मेदार लोकसेवकों से ही वसूल करना राज्य की जिम्मेदारी है।
सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट शब्दों में कहा है कि जिन व्यक्तियों के कारण नागरिकों के संवैधानिक अधिकारों का उल्लंघन हुआ है — उनमें न्यायाधीश भी शामिल हैं — उनसे ही अंततः यह क्षतिपूर्ति वसूल की जानी चाहिए।
सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय
यह महत्वपूर्ण सिद्धांत सर्वोच्च न्यायालय ने निम्नलिखित मामलों में रेखांकित किया है :
- Directions in the Matter of Demolition of Structures, In re, (2025) 5 SCC 1
- Lucknow Development Authority v. M.K. Gupta, AIR 1994 SC 787
इन निर्णयों में न्यायालय ने स्पष्ट रूप से कहा है कि जनता के पैसों से गलत आदेशों की भरपाई करना अन्याय है और दोषी न्यायाधीशों तथा अधिकारियों से ही क्षतिपूर्ति वसूल की जानी चाहिए।
पाँच न्यायाधीशों की खंडपीठ द्वारा अवमान प्रकरण में दिया गया आदेश पहले से ही रद्दबातल (overruled) व अप्रचलित ठहराए गए निर्णयों पर आधारित है
यह ठोस आरोप लगाया गया है कि पाँच न्यायाधीशों की खंडपीठ द्वारा अवमान प्रकरण में दिया गया आदेश पहले से ही रद्दबातल (overruled) व अप्रचलित ठहराए गए निर्णयों पर आधारित है। यह आदेश केवल आरोपी न्यायमूर्ति श्रीमती रेवती मोहिते डेरे को बचाने के लिए, तथा सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ द्वारा निर्धारित कानून के प्रत्यक्ष विरोध में पारित किया गया है, इसलिए यह आदेश पूर्णतः अवैध है।
याचिकाकर्ता अधिवक्ता को न्यायमूर्ति श्रीमती रेवती मोहिते डेरे के गैरकृत्यों को सार्वजनिक रूप से उजागर करने के कारण स्कैंडलस प्लीडिंग (scandalous pleading) के आधार पर अवमान का दोषी ठहराने हेतु उच्च न्यायालय ने Andre Paul Terence Ambard v. Attorney-General of Trinidad and Tobago, 1936 SCC OnLine PC 15 तथा Sanjiv Datta, Dy. Secy., Ministry of Information & Broadcasting, In re, (1995) 3 SCC 619 जैसे पहले से रद्दबातल (overruled) ठहराए गए निर्णयों का सहारा लिया।
इसमें सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ तथा अन्य मामलों में दिए गए निम्नलिखित बंधनकारी न्यायनिदर्शकों (binding precedents) का प्रत्यक्ष उल्लंघन किया गया है :
- Subramanian Swamy v. Arun Shourie, (2014) 12 SCC 344
- C.S. Karnan, In re, (2017) 2 SCC 756
- Indirect Tax Practitioners’ Assn. v. R.K. Jain, (2010) 8 SCC 281
- Re Lalit Kalita, (2008) 1 Gau LT 800
- Bathina Ramakrishna Reddy v. State of Madras, 1952 SCR 425
- Hari Das v. State of W.B., (1964) 7 SCR 237
भारत में स्थिर कानूनी स्थिति
भारत में कानून की स्थिर और स्पष्ट स्थिति, जो संविधान पीठ (Constitution Benches) सहित अनेक निर्णयों में प्रतिपादित की गई है, इस प्रकार है :
**“जब किसी न्यायाधीश पर आपराधिक अपराध, भ्रष्टाचार या गंभीर कदाचार के आरोप होते हैं, तब शिकायत, याचिका या प्रतिवेदन में ऐसे न्यायाधीश पर दुर्भावनापूर्ण आचरण के आरोप लगाना — अथवा सच्चे तथ्यों पर आधारित समाचार प्रकाशित करना — न केवल अनुमत है बल्कि व्यापक लोकहित के लिए आवश्यक भी है।
यह करना प्रत्येक नागरिक का संवैधानिक कर्तव्य (अनुच्छेद 51-अनुसार) तथा प्रत्येक अधिवक्ता का वैधानिक कर्तव्य (बार काउंसिल ऑफ इंडिया नियमों के अनुसार) है, ताकि भ्रष्ट तत्वों से न्यायदान प्रणाली की शुचिता सुरक्षित रहे और न्यायालयों की गरिमा कलंकित न हो।
ऐसे पवित्र कर्तव्य का पालन करने वाले व्यक्ति वास्तव में ‘व्हिसलब्लोअर’ हैं; उन्हें संविधान के अनुच्छेद 129 और 215 या अवमान अधिनियम, 1971 के अंतर्गत चुप नहीं कराया जा सकता। इसके विपरीत, जो लोग अवमानाधिकार का दुरुपयोग कर ऐसे व्हिसलब्लोअर के विरुद्ध कार्यवाही करते हैं, उन्हें ही कठोर दंड दिया जाना चाहिए और उन पर उदाहरणीय खर्च (exemplary costs) भी लगाया जाना चाहिए।
यदि कोई व्यक्ति झूठे या तुच्छ अवमान आरोप लगाता है, तो वह स्वयं ही भारतीय दंड संहिता की धारा 211 के अंतर्गत दंडनीय अपराध का दोषी है।
इसके अतिरिक्त, कोई भी न्यायाधीश यदि जानबूझकर बंधनकारी न्यायनिदर्शकों की उपेक्षा करता है, दुर्भावनापूर्ण तरीके से कार्य करता है या अवमानाधिकार का दुरुपयोग करता है, तो उस पर भारतीय दंड संहिता की धाराएँ 219, 220, 166 और अन्य संबंधित प्रावधानों के अंतर्गत आपराधिक दायित्व निश्चित किया जा सकता है।”