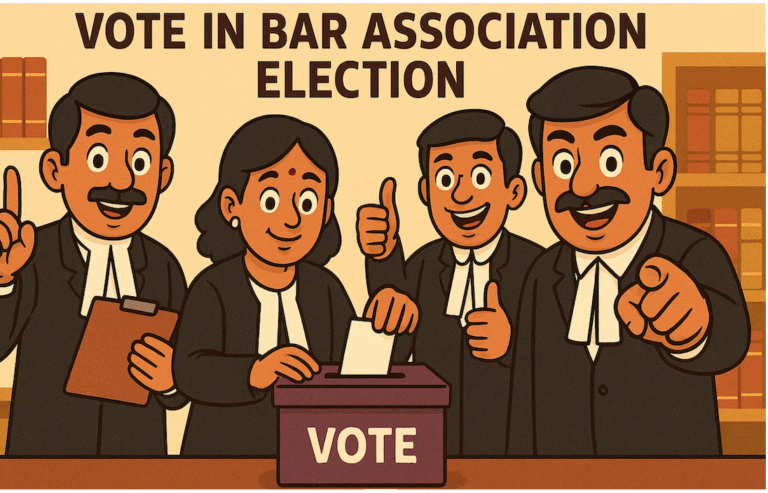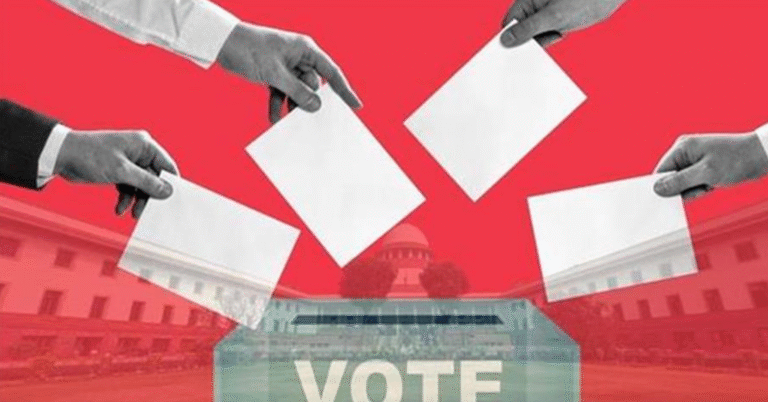बॉम्बे हाईकोर्ट के मुख्य न्यायमूर्ति चंद्रशेखर गंभीर मुश्किल में!

राष्ट्रपति सचिवालय ने पेन ड्राइव सहित शिकायत न्याय मंत्रालय को कार्रवाई के लिए भेजी; ₹7.5 करोड़ मुआवजे की याचिका पर सुनवाई से न्यायमूर्ति गडकरी ने खुद को अलग किया!
बॉम्बे हाईकोर्ट के मुख्य न्यायमूर्ति श्री चंद्रशेखर के खिलाफ दाखिल हुई गंभीर शिकायत ने पूरे न्यायिक गलियारों में हलचल मचा दी है।
राष्ट्रपति सचिवालय ने सबूतों से भरी पेन ड्राइव सहित यह शिकायत न्याय विभाग (Department of Justice) को आगे की कार्रवाई के लिए भेज दी है।
सूत्रों के अनुसार, यह शिकायत दिशा सालियान के पिता श्री सतीश सालियान और इंडियन लॉयर्स एंड ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट्स एसोसिएशन द्वारा दाखिल की गई है। शिकायत में आरोप लगाया गया है कि मुख्य न्यायमूर्ति चंद्रशेखर ने न्यायमूर्ति सी. एस. कर्णन की राह अपनाते हुए भारतीय संविधान और सर्वोच्च न्यायालय के आदेशों को ठुकरा दिया है।
शिकायत के मुताबिक, मुख्य न्यायमूर्ति चंद्रशेखर ने सर्वोच्च न्यायालय के बंधनकारी दिशा-निर्देशों का खुला उल्लंघन करते हुए मनमाने आदेश पारित किए।
उन्होंने अदालत में खुले तौर पर कहा कि — “वे पक्षकारों या उनके वकीलों को सुनने, उनके तर्क या निवेदन पर विचार करने, या कारणयुक्त (reasoned) आदेश देने के लिए बाध्य नहीं हैं।”
सबसे चौंकाने वाली बात यह बताई गई है कि उन्होंने कहा —
“अगर कोई वकील सर्वोच्च न्यायालय के निर्णयों का हवाला देगा या उन पर आधारित तर्क पेश करेगा, तो उसे हिरासत में लिया जाएगा!”
कानूनी विशेषज्ञों के अनुसार, यह आचरण भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14, 21 और 141 का सीधा उल्लंघन है। उल्लेखनीय है कि ऐसे ही आचरण के लिए न्यायमूर्ति सी. एस. कर्णन को सर्वोच्च न्यायालय ने छह महीने की सजा सुनाई थी।
कानूनी हलकों में यह मामला “भारतीय न्यायपालिका के इतिहास का सबसे गंभीर घटनाक्रम” माना जा रहा है और अब सबकी निगाहें न्याय मंत्रालय और राष्ट्रपति भवन की आगामी कार्रवाई पर टिक गई हैं।
मुख्य न्यायमूर्ति चंद्रशेखर ने नकारा संविधान का सिद्धांत — ‘कानून के सामने सब समान’ की भावना को ठेस!
न्यायमूर्ति गडकरी के फैसले ने फिर उजागर किया मुख्य न्यायमूर्ति चंद्रशेखर का मनमाना और असंवैधानिक रवैया
मुख्य न्यायमूर्ति चंद्रशेखर पर गंभीर आरोपों की झड़ी लग गई है।
उन्होंने सर्वोच्च न्यायालय के बाध्यकारी निर्णयों को न मानते हुए, संविधान द्वारा प्रदत्त मूल सिद्धांत — “कानून के सामने सब समान” — को ही नकार दिया है।
कानूनी विशेषज्ञों के अनुसार, उनका यह व्यवहार न्यायपालिका की संवैधानिक अनुशासन, न्यायिक नैतिकता और वकालत की स्वतंत्रता पर सीधा प्रहार है।
इस पूरे घटनाक्रम को लेकर न्यायिक और विधिक हलकों में गहरी नाराज़गी और चिंता की लहर देखी जा रही है।
न्यायमूर्ति गडकरी के फैसले ने फिर उजागर किया मुख्य न्यायमूर्ति चंद्रशेखर का असंवैधानिक व्यवहार
4 नवंबर 2025 को मुख्य न्यायमूर्ति चंद्रशेखर के खिलाफ दायर याचिका पर सुनवाई के दौरान, न्यायमूर्ति ए. एस. गडकरी ने एक अत्यंत संवेदनशील और नैतिक निर्णय लिया।
उन्होंने ‘हितों के टकराव’ (Conflict of Interest) का हवाला देते हुए स्वयं को इस मामले की सुनवाई से अलग कर लिया। उनके इस कदम की कानूनी हलकों में व्यापक सराहना हुई है, क्योंकि इससे न्यायिक निष्पक्षता, अनुशासन और पारदर्शिता के सर्वोच्च मानक कायम रहे।
🔴 लेकिन सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि,
मुख्य न्यायमूर्ति चंद्रशेखर ने खुद पर आरोप होने के बावजूद अपने ही खिलाफ मामले की सुनवाई की, और खुद को उस प्रकरण से अलग करने से साफ इंकार कर दिया।
कानूनी जगत का मानना है कि, न्यायमूर्ति गडकरी के इस संयमित और नैतिक निर्णय ने एक बार फिर मुख्य न्यायमूर्ति चंद्रशेखर का अहंकारी, अवैध और असंवैधानिक रवैया उजागर कर दिया है।
यह घटना न केवल न्यायपालिका की निष्पक्षता पर प्रश्नचिह्न खड़ा करती है,
बल्कि यह दिखाती है कि संविधान और न्यायिक आचारसंहिता की सीमाओं को लांघने का साहस किसी न्यायिक पद पर बैठे व्यक्ति को भी नहीं होना चाहिए।
राष्ट्रपति सचिवालय ने छह दिन की जांच के बाद डिजिटल साक्ष्यों सहित (पेन ड्राइव में अदालत के रिकॉर्ड, कार्यवाही और वीडियो सामग्री) मौजूद शिकायत को न्याय विभाग की निदेशक श्रीमती राधा कट्याल नारंग को आवश्यक कार्रवाई हेतु भेज दिया है।
यह मामला न्यायिक जगत में बड़ा भूचाल लेकर आया है। इस प्रकरण में 15 वकीलों ने मिलकर ₹7.5 करोड़ के मुआवजे की याचिका दायर की है। वकीलों का आरोप है कि मुख्य न्यायमूर्ति चंद्रशेखर ने सर्वोच्च न्यायालय के बाध्यकारी आदेशों और निषेधात्मक निर्देशों की खुली अवहेलना करते हुए अवैध आदेश पारित किए, जिससे उनके मौलिक अधिकारों का गंभीर हनन हुआ।
इस याचिका पर सुनवाई के दौरान, न्यायमूर्ति ए. एस. गडकरी ने “हितों के टकराव (Conflict of Interest)” का हवाला देते हुए स्वयं को इस मामले की सुनवाई से अलग कर लिया।
उनके इस निर्णय की न्यायिक हलकों में निष्पक्षता और पारदर्शिता के आदर्श उदाहरण के रूप में सराहना की जा रही है।
मुख्य न्यायमूर्ति चंद्रशेखर जैसे न्यायाधीशों के खिलाफ कार्रवाई की पृष्ठभूमि में, सर्वोच्च न्यायालय ने हाल के कई मामलों में न्यायिक अयोग्यता, मनमानी और कानून की समझ की कमी पर कड़ी टिप्पणियां की हैं।
1. Shikhar Chemicals v. State of U.P., 2025 SCC OnLine SC 1653 —
इस मामले में न्यायमूर्ति जे. बी. पार्डीवाला ने एक हाईकोर्ट के न्यायाधीश की कमजोर कानूनी समझ और गैर-जिम्मेदाराना दृष्टिकोण की कड़ी आलोचना की।
उन्होंने संबंधित मुख्य न्यायाधीश को आदेश दिया कि,
“ऐसे न्यायाधीश को कोई न्यायिक कार्य न दिया जाए, क्योंकि कानून का बुनियादी ज्ञान न होना न्यायपालिका की विश्वसनीयता पर कलंक है।”
2. Court on its Own Motion v. Jayant Kashmiri, 2017 SCC OnLine Del 7387 —
दिल्ली हाईकोर्ट ने एक ऐसे न्यायाधीश को फटकार लगाई जिसने केवल सर्वोच्च न्यायालय का फैसला दिखाने वाले वकील के खिलाफ अवमानना शुरू कर दी थी।
अदालत ने कहा —
“न्यायाधीश ने अवमान अधिकार का दुरुपयोग किया है और उसे कानून की प्रकृति समझने के लिए न्यायिक प्रशिक्षण की आवश्यकता है।”
3. Hakim Nazir Ahmad v. Commissioner, 2025 SCC OnLine J&K ___ —
इस प्रकरण में न्यायाधीश ने बिना कोई कारण दर्ज किए याचिका खारिज कर दी।
अदालत ने कठोर टिप्पणी करते हुए कहा कि, “उक्त न्यायाधीश को यह भी नहीं पता कि आदेश कैसे लिखा जाए और कारणमीमांसा क्या होती है।” इसके बाद उसे न्यायिक प्रशिक्षण के आदेश दिए गए।
4. P. Radhakrishnan v. Cochin Devaswom Board, 2025 SCC OnLine SC 2118 —
सर्वोच्च न्यायालय ने सभी न्यायाधीशों को चेताया कि, “ऐसे आदेश जो पक्षकारों या वकीलों को भयभीत करें या न्याय की प्रक्रिया पर ठंडा असर डालें, वे विधि के शासन के लिए गंभीर खतरा हैं।”
इन उदाहरणों के आलोक में, कानूनी विशेषज्ञों का मानना है कि मुख्य न्यायमूर्ति चंद्रशेखर का आचरण भी इन्हीं गंभीर श्रेणियों में आता है, और उनके खिलाफ संवैधानिक तथा दंडात्मक कार्रवाई अब अपरिहार्य प्रतीत होती है।
मुख्य न्यायमूर्ति चंद्रशेखर पर यह गंभीर आरोप लगाया गया है कि उन्होंने वकीलों द्वारा दाखिल किए गए अर्जों की लंबाई और उनके द्वारा प्रस्तुत किए गए न्यायनिर्णयों की संख्या पर आपत्ति जताई, और इसी आधार पर उन्होंने वकीलों को “हिरासत में लेने की धमकी” दी।
यह रवैया सर्वोच्च न्यायालय की न्यायमूर्ति जे. बी. पार्डीवाला की अध्यक्षता वाली पीठ के फैसले Amrish Rajnikant Kilachand v. Secretary General, Supreme Court of India, 2023 SCC OnLine SC 2511 — में घोषित स्पष्ट कानून के प्रत्यक्ष उल्लंघन के समान है।
उस निर्णय में सर्वोच्च न्यायालय ने स्पष्ट कहा था कि —
“न्यायालय किसी भी पक्षकार द्वारा दाखिल की गई याचिकाओं के पृष्ठों या लंबाई पर कोई प्रतिबंध नहीं लगा सकता।”
कानून का स्थापित सिद्धांत यह है कि यदि अदालत को याचिका अत्यधिक लंबी या जटिल लगे, तो वह पक्षकारों को एक संक्षिप्त लिखित सारांश या बिंदुवार विवरण प्रस्तुत करने का निर्देश दे सकती है, परंतु वह वकीलों के इस वैध अधिकार को सीमित नहीं कर सकती कि वे अपने पक्ष में आवश्यक कानूनी उदाहरण या निर्णय प्रस्तुत करें।
इसी प्रकार, सर्वोच्च न्यायालय ने Bar Council of India v. High Court of Kerala, (2004) 6 SCC 311 में सख्त चेतावनी दी थी कि —
“अवमान अधिकार न्यायपालिका का वह क्षेत्र है, जिसका सबसे अधिक दुरुपयोग और गलत अर्थ लगाया जाता है। इस अधिकार का इस्तेमाल वकीलों को डराने या उनकी वैध वकालत की स्वतंत्रता पर अंकुश लगाने के लिए नहीं किया जा सकता।”
सर्वोच्च न्यायालय ने यह भी दोहराया है कि
“हर पक्षकार का यह कर्तव्य है कि वह अदालत के समक्ष सभी बाध्यकारी निर्णय — चाहे वे उसके पक्ष में हों या विरुद्ध — प्रस्तुत करे। इन निर्णयों को जानबूझकर छिपाना व्यावसायिक दुराचार (Professional Misconduct) माना जाएगा।”
लेकिन इसके पूरी तरह विपरीत, मुख्य न्यायमूर्ति चंद्रशेखर ने एक चौंकाने वाला और असंवैधानिक रवैया अपनाया — उन्होंने उन वकीलों को ही दंडित करने और डराने का प्रयास किया, जो अपने तर्कों के समर्थन में सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय प्रस्तुत कर रहे थे।
यह रवैया न केवल संविधान के अनुच्छेद 14, 19(1)(g) और 21 का उल्लंघन है,
बल्कि न्यायपालिका की स्वतंत्रता, जवाबदेही और नैतिक मर्यादा पर सीधा प्रहार भी है। इसने पूरे कानूनी समुदाय में गहरा आक्रोश पैदा कर दिया है — जहां वरिष्ठ अधिवक्ता और न्यायविद यह कह रहे हैं कि
“अगर सर्वोच्च न्यायालय के निर्णयों को उद्धृत करने वाले वकील ही अपराधी ठहराए जाएंगे,
तो यह न्याय नहीं, बल्कि न्यायपालिका पर अधिनायकवाद की छाया है।”
इस घटनाक्रम ने न्यायिक प्रणाली में संवैधानिक अनुशासन और न्यायिक जिम्मेदारी को लेकर
गंभीर प्रश्न खड़े कर दिए हैं, और अब मांग उठ रही है कि मुख्य न्यायमूर्ति चंद्रशेखर के विरुद्ध अनुशासनात्मक और आपराधिक कार्रवाई की जाए।
न्यायिक पद का दुरुपयोग और न्यायिक नैतिकता का उल्लंघन :
1. याचिकाकर्ताओं ने मुख्य न्यायमूर्ति चंद्रशेखर के खिलाफ फौजदारी मुकदमा दर्ज करने की मांग की है। यह मांग भारतीय न्याय संहिता (BNS) और Contempt of Courts Act के अंतर्गत की गई है, जिसमें निम्नलिखित गंभीर आरोप लगाए गए हैं —
(A) अधिकारों का जानबूझकर दुरुपयोग और न्यायिक मर्यादा का अभाव,
(B) वकीलों के साथ अहंकारी और असभ्य व्यवहार,
(C) मूलभूत कानूनों का अपर्याप्त ज्ञान और संविधान की धाराओं का गलत अर्थ,
(D) सर्वोच्च न्यायालय के बाध्यकारी निर्णयों का जानबूझकर उल्लंघन, और
(E) अभियुक्तों को बचाने के लिए कानूनी आवेदन और बाध्यकारी फैसलों को दबाने का प्रयास।
2. यह भी गंभीर आरोप लगाया गया है कि मुख्य न्यायमूर्ति चंद्रशेखर ने वकीलों को यह धमकी दी — “यदि उन्होंने सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय दिखाए या उन पर आधारित आवेदन किए, तो उन्हें हिरासत में लिया जाएगा।” यह रवैया स्वयं सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निर्धारित स्पष्ट कानून के सीधे उल्लंघन के समान है।
संबंधित निर्णय इस प्रकार हैं —
• State of U.P. v. Association of Retired Supreme Court & High Court Judges, (2024) 3 SCC 1
• P.K. Ghosh v. J.G. Rajput, (1995) 6 SCC 744
• Chetak Construction Ltd. v. Om Prakash, (1998) 4 SCC 577
3. इन सभी निर्णयों में सर्वोच्च न्यायालय ने स्पष्ट किया है कि —यदि कोई वकील या पक्षकार किसी आदेश को अवैध या त्रुटिपूर्ण बताते हुए उसके पुनर्विचार (Recall Application) की मांग करता है, या किसी न्यायाधीश के हितों के टकराव (Conflict of Interest) को लेकर Recusal Application दाखिल करता है,
तो यह उसका संवैधानिक और वैध अधिकार है।
ऐसे आवेदन करने वाले वकील या पक्षकार को सज़ा देना, धमकाना या अवमानना की कार्रवाई करना न्यायिक शक्तियों का दुरुपयोग माना जाएगा।
4. सर्वोच्च न्यायालय ने यह भी स्पष्ट किया है कि “अदालत में गिरफ्तारी या हिरासत में लेने की शक्ति केवल अपवादस्वरूप स्थितियों में प्रयोग की जा सकती है —
जैसे कि शारीरिक हमला, अभद्र भाषा या अपमानजनक व्यवहार की स्थिति में।
केवल कानूनी आवेदन दाखिल करना या न्यायालय के निर्णयों का हवाला देना कभी अपराध नहीं हो सकता।”
5. Mehmood Pracha v. Central Administrative Tribunal, (2022) SCC OnLine SC 1029 में सर्वोच्च न्यायालय ने सख्त शब्दों में कहा — “वकील द्वारा कानूनी आवेदन दाखिल करना, सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय प्रस्तुत करना
या विधिक स्थिति पर जोर देना — इन कारणों से गिरफ्तारी करना पूर्णतः न्यायिक अधिकारों का दुरुपयोग है।”
6. इन सभी स्पष्ट दिशा-निर्देशों की पूर्ण अवहेलना करते हुए,
मुख्य न्यायमूर्ति चंद्रशेखर ने केवल सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय प्रस्तुत करने पर ही
वकीलों को गिरफ्तार करने की धमकी दी।
7. यह कृत्य न्यायिक शक्ति का गंभीर और जानबूझकर किया गया दुरुपयोग है,
जो न्यायिक अधिकारों के खुले उल्लंघन और संस्थागत अनुशासन के पतन का प्रतीक माना जा रहा है।
8. सुप्रीम कोर्ट के दिशा-निर्देशों का उल्लंघन — वकीलों के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणी :- शिकायत के अनुसार, 17 सितंबर 2025 के आदेश में मुख्य न्यायमूर्ति चंद्रशेखर ने 15 वकीलों के खिलाफ उनकी अनुपस्थिति में अपमानजनक और मानहानिकारक टिप्पणियाँ कीं, और उन्हें अपना पक्ष रखने या सफाई देने का कोई अवसर नहीं दिया।
9. यह आचरण सुप्रीम कोर्ट के स्पष्ट दिशा-निर्देशों का उल्लंघन है।
सुप्रीम कोर्ट ने Dushyant Mainali v. Diwan Singh Bora, 2024 SCC OnLine SC 5178, और Neeraj Garg v. Sarita Rani, (2021) 9 SCC 92 मामलों में स्पष्ट रूप से कहा है कि — “कोई भी न्यायाधीश किसी वकील के खिलाफ नकारात्मक या अपमानजनक टिप्पणी करने से पहले
उसे सुनने और अपनी बात रखने का उचित अवसर अवश्य दे।” मुख्य न्यायमूर्ति चंद्रशेखर ने इस सिद्धांत की पूरी तरह अनदेखी करते हुए
एकतरफा आदेश पारित किया, जिससे वकीलों की इज़्ज़त, सम्मान और पेशेवर गरिमा को ठेस पहुँची। यह कृत्य न्यायिक शिष्टाचार और नैतिकता के मूलभूत सिद्धांतों का घोर उल्लंघन है।
10. आरोप संख्या 7 — बाध्यकारी निर्णयों और बड़ी पीठों के फैसलों की कानूनी समझ का अभाव : – मुख्य न्यायमूर्ति चंद्रशेखर पर यह गंभीर आरोप लगाया गया है कि उन्हें बाध्यकारी निर्णयों (Binding Precedents), ‘Per Incuriam’ निर्णयों और ‘Overruled’ निर्णयों की मौलिक कानूनी समझ नहीं है। उन्होंने विधिशास्त्र के उस स्थापित सिद्धांत की उपेक्षा की कि — “बड़ी पीठ का निर्णय हमेशा छोटी पीठ के निर्णय पर प्राथमिकता रखता है।”
11. इस स्थापित सिद्धांत के विपरीत, मुख्य न्यायमूर्ति चंद्रशेखर ने Pritam Pal v. High Court of Madhya Pradesh (दो न्यायाधीशों की पीठ द्वारा दिया गया और बाद में रद्द किया गया निर्णय) पर भरोसा किया, जबकि उन्होंने बड़े पीठों के स्पष्ट और बाध्यकारी निर्णयों को जानबूझकर नजरअंदाज किया, जैसे —
• Bal Thackeray v. Pimplekhute, (2005) 1 SCC 254
• Dr. L.P. Misra v. State of U.P., (1998) 7 SCC 379
• Pallav Sheth v. Custodian, (2001) 7 SCC 549
12. इस रवैये से न केवल मुख्य न्यायमूर्ति चंद्रशेखर की न्यायिक क्षमता और कानूनी समझ पर प्रश्नचिह्न लगा है, बल्कि उनके आचरण ने न्यायपालिका की शुचिता, अनुशासन और कानून की सर्वोच्चता के सिद्धांत को गहरी ठेस पहुँचाई है।
13. न्यायिक अधिकार क्षेत्र से बाहर जाकर पारित आदेश — सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ के निर्देशों का उल्लंघन :
(Supreme Court Bar Association v. Union of India, (1998) 4 SCC 409)
14. मुख्य न्यायमूर्ति चंद्रशेखर पर यह गंभीर आरोप लगाया गया है कि उन्होंने 15 वकीलों के खिलाफ कथित व्यावसायिक दुर्व्यवहार (Professional Misconduct) के मामले में एकतरफा (Ex-Parte) और अवैध दोषसिद्धि आदेश जारी किया।
यह आदेश सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ (Constitution Bench) द्वारा दिए गए ऐतिहासिक निर्णय Supreme Court Bar Association v. Union of India, (1998) 4 SCC 409 के सीधे विरोध में है।
15. उक्त ऐतिहासिक निर्णय में सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट शब्दों में कहा था कि — “न तो उच्च न्यायालय और न ही सर्वोच्च न्यायालय को किसी वकील के पेशेवर आचरण (Professional Misconduct) पर कोई निष्कर्ष दर्ज करने या दंड देने का अधिकार है। इस प्रकार की अनुशासनात्मक कार्यवाही का अधिकार केवल और केवल बार काउंसिल ऑफ इंडिया (Bar Council of India) को है,
और यह प्रक्रिया Advocates Act, 1961 के तहत बार काउंसिल की अनुशासन समिति (Disciplinary Committee) के अधिकार क्षेत्र में आती है।”
16. इस प्रकार, मुख्य न्यायमूर्ति चंद्रशेखर द्वारा पारित किया गया यह आदेश
संवैधानिक सीमाओं का खुला उल्लंघन है और
सुप्रीम कोर्ट के बाध्यकारी निर्णय की प्रत्यक्ष अवहेलना का प्रतीक है।
17. यह कृत्य न केवल न्यायिक अनुशासन और मर्यादा के विपरीत है,
बल्कि न्यायिक सत्ता के मनमाने उपयोग और संविधान के प्रति घोर उदासीनता का
एक गंभीर और निंदनीय उदाहरण प्रस्तुत करता है।
18. मुख्य न्यायमूर्ति चंद्रशेखर का विवादास्पद आदेश : सुप्रीम कोर्ट के कानून की खुली अवहेलना :- न्यायमूर्ति चंद्रशेखर के 16 अक्टूबर 2025 के आदेश ने न्यायिक और विधिक जगत में तूफान खड़ा कर दिया है।
इस आदेश में उन्होंने याचिकाकर्ताओं के सभी तर्क और प्रार्थनाएँ सुने बिना, किसी भी प्रकार का कारण दर्ज किए बगैर याचिका को सीधे खारिज कर दिया।
इतना ही नहीं, उन्होंने अपने आदेश में यह तक लिख दिया — “सभी मुद्दों और प्रार्थनाओं पर विचार करना कानूनन अनिवार्य नहीं है।”
19. कानूनी विशेषज्ञों के अनुसार, यह रुख सुप्रीम कोर्ट के बाध्यकारी निर्णयों की खुली अवहेलना है। Vishal Ashwin Patel v. CIT, (2022) 14 SCC 817 में सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट कहा है —
“कारण सहित आदेश (Reasoned Order) न्यायिक निर्णय की आत्मा है। हर अदालत को पक्षकारों द्वारा उठाए गए सभी मुद्दों पर विचार कर स्पष्ट कारण देने चाहिए। न्याय में पारदर्शिता और विश्वास इसी पर आधारित है।”
20. विडंबना यह है कि, कुछ महीने पहले मुख्य न्यायमूर्ति चंद्रशेखर ने स्वयं ही
Registrar, Nilamber Pitamber University v. State of Jharkhand, 2023 SCC OnLine Jhar 1635 मामले में यह लिखा था — “कारण सहित आदेश के बिना न्याय संभव नहीं है।” लेकिन अब उन्होंने अपने ही शब्दों से पलटी मारते हुए इसके विपरीत निर्णय दिया, जिससे यह स्पष्ट होता है कि उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के कानून और संविधान के मूल सिद्धांतों की अनदेखी की है। कानूनी हलकों में इसे “जानबूझकर किया गया न्यायिक विरोधाभास” और “संवैधानिक शपथ का उल्लंघन” बताया जा रहा है।
21. वकीलों के बीच यह चर्चा है कि मुख्य न्यायमूर्ति चंद्रशेखर का यह रवैया अहंकार, मनमानी और कानून के प्रति उदासीनता का जीवंत उदाहरण बन गया है।
कानूनी विशेषज्ञों का मानना है — “यह मामला अनुच्छेद 14 के तहत समानता के सिद्धांत का उल्लंघन और न्यायपालिका की आत्मा पर प्रहार है।”
⚖️ क्या मुख्य न्यायमूर्ति चंद्रशेखर चल पड़े न्यायमूर्ति सी. एस. कर्णन के रास्ते पर?
1. शिकायत के अनुसार, मुख्य न्यायमूर्ति चंद्रशेखर ने न्यायमूर्ति सी. एस. कर्णन का रास्ता अपनाया है। उन्होंने भारतीय संविधान और सुप्रीम कोर्ट के आदेशों को दरकिनार करते हुए, सुप्रीम कोर्ट की बंधनकारी दिशानिर्देशों का खुला उल्लंघन किया है। उन्होंने अदालत में खुले तौर पर घोषणा की कि — “वे न तो पक्षकारों को सुनने के लिए बाध्य हैं, न उनकी दलीलों या प्रार्थनाओं पर विचार करने के लिए, और न ही कारण सहित आदेश देने के लिए।”
2. इससे भी अधिक चौंकाने वाली बात यह है कि उन्होंने कहा — “अगर कोई वकील सुप्रीम कोर्ट के निर्णयों का हवाला देगा या उन पर भरोसा करेगा, तो उसे हिरासत में लिया जाएगा!”
3. यह बयान न्यायपालिका की संवैधानिक मर्यादा, न्यायिक नैतिकता और वकालत की स्वतंत्रता पर सीधा हमला माना जा रहा है, और कानूनी जगत में मुख्य न्यायमूर्ति चंद्रशेखर के इस व्यवहार को लेकर गहरा आक्रोश और चिंता व्यक्त की जा रही है।
4. कानूनी विशेषज्ञों की प्रतिक्रिया — न्यायपालिका में मचा हड़कंप :- कानूनी विशेषज्ञों का कहना है कि यह घटना “भारतीय न्यायव्यवस्था के इतिहास की सबसे शर्मनाक और अभूतपूर्व घटनाओं में से एक” है।
न्यायमूर्ति चंद्रशेखर के इस रवैये ने संविधान का अपमान, न्यायिक अनुशासन का उल्लंघन और सुप्रीम कोर्ट के अधिकार को खुली चुनौती दी है।
एक वरिष्ठ अधिवक्ता ने कहा — “यदि इस मामले में तुरंत कार्रवाई नहीं हुई, तो जनता का न्यायपालिका पर से विश्वास पूरी तरह समाप्त हो जाएगा।”
5. मुख्य न्यायमूर्ति चंद्रशेखर के खिलाफ दो अलग-अलग शिकायतें दाखिल:- राष्ट्रपति सचिवालय में दो स्वतंत्र शिकायतें दर्ज हुई हैं —
(i) दिशा सालियन के पिता श्री सतीश सालियन द्वारा दर्ज की गई शिकायत — प्रकरण संख्या PRSEC/E/2025/0061948, जो वर्तमान में राष्ट्रपति सचिवालय में परीक्षणाधीन है।
(ii) इंडियन लॉयर्स एंड ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट्स एसोसिएशन (ILHRA) द्वारा दर्ज की गई शिकायत — 1 नवंबर 2025 को प्राप्त होकर फाइल संख्या PRSEC/E/2025/0061483 के तहत दर्ज की गई है।
6. यह शिकायत 7 नवंबर 2025 को न्याय मंत्रालय (Department of Justice) को आगे की कानूनी व प्रशासनिक कार्रवाई हेतु प्रेषित की गई है।
7. दोनों शिकायतें शपथपत्र (Affidavit) के साथ दायर की गई हैं,
जिनमें डिजिटल सबूत — जैसे पेन ड्राइव में न्यायिक कार्यवाही, रिकॉर्ड्स और वीडियो सामग्री — संलग्न हैं। इन दोनों शिकायतों से न्यायिक हलकों में बड़ी हलचल मच गई है, और सूत्रों के अनुसार, न्याय मंत्रालय इस मामले को अत्यंत गंभीरता से जांच रहा है।
8. सुप्रीम कोर्ट द्वारा स्थापित सिद्धांत — दोषी न्यायाधीशों पर कठोर अनुशासनात्मक व आपराधिक कार्रवाई.
9. सुप्रीम कोर्ट और विभिन्न उच्च न्यायालयों ने अतीत में ऐसे ही मामलों में,
जहां न्यायाधीशों ने संवैधानिक शपथ का उल्लंघन, न्यायिक शक्तियों का दुरुपयोग या न्यायिक आचरण का हनन किया,
वहां कठोर और स्पष्ट कानूनी सिद्धांत निर्धारित किए हैं।
इन निर्णयों ने न्यायपालिका में शुचिता, पारदर्शिता और जवाबदेही की ठोस रूपरेखा स्थापित की है।
10. मुख्य न्यायमूर्ति चंद्रशेखर पर लगे आरोप —
👉 न्यायिक अधिकारों का जानबूझकर दुरुपयोग,
👉 न्यायालय की अवमानना (Contempt of Court),
👉 संवैधानिक सीमाओं का उल्लंघन,
👉 निष्पक्षता की कमी, तथा
👉 संविधान के अनुरूप समान न्याय लागू न करना —
ये सभी आरोप उन मामलों से मेल खाते हैं, जिनमें सुप्रीम कोर्ट ने न्यायाधीशों को दोषी ठहराकर सजा दी थी।
11. सुप्रीम कोर्ट ने Re: Justice C.S. Karnan, (2017) 7 SCC 1 में कहा था —
“जो न्यायाधीश सुप्रीम कोर्ट के आदेशों की अवहेलना करता है, न्यायसंहिता से ऊपर स्वयं को रखता है या जनता के न्यायिक विश्वास को कमजोर करता है,
उस पर अवमानना और आपराधिक कार्रवाई आवश्यक है।”
12. इसी प्रकार R.R. Parekh v. High Court of Gujarat, (2016) 14 SCC 1 तथा Prabha Sharma v. Sunil Goyal, (2017) 11 SCC 77 में सुप्रीम कोर्ट ने कहा —
“न्यायिक शक्ति व्यक्तिगत प्रतिष्ठा नहीं, बल्कि सार्वजनिक विश्वास और संवैधानिक जिम्मेदारी का साधन है; यदि इसका दुरुपयोग हो, तो दंड अपरिहार्य है।”
ऐसे मामलों में न्यायालयों ने —
• कोर्ट-अवमानना की कार्रवाई की,
• न्यायिक कार्य तत्काल वापस लिए,
• विभागीय जांच और निलंबन आदेश जारी किए,
• और कुछ मामलों में आपराधिक मुकदमे चलाकर न्यायाधीशों को निलंबित या सेवानिवृत्त किया।
सुप्रीम कोर्ट का सिद्धांत :
“न्यायाधीश संविधान का सेवक होता है; उसका अधिकार असीम नहीं, बल्कि जवाबदेही से सीमित है। यदि कोई न्यायाधीश अपनी शपथ का उल्लंघन करता है और जनता के विश्वास को तोड़ता है, तो न्यायपालिका स्वयं अपनी शुचिता और गरिमा की रक्षा के लिए उस पर कार्रवाई करने की बाध्य है।”
कानूनी विशेषज्ञों का मानना है कि मुख्य न्यायमूर्ति चंद्रशेखर के खिलाफ लगाए गए आरोप
उपरोक्त सभी उदाहरणों की तुलना में कहीं अधिक गंभीर और प्रत्यक्ष रूप से सिद्ध होने वाले हैं।इसी कारण, उनके विरुद्ध कानून मंत्रालय, सर्वोच्च न्यायालय की संविधान पीठ और सीबीआई द्वारासंयुक्त रूप से अनुशासनात्मक कार्रवाई, निलंबन, बर्खास्तगी और आपराधिक मुकदमा चलानान्यायव्यवस्था की विश्वसनीयता और संविधानिक मर्यादा बनाए रखने के लिए अत्यावश्यक और अपरिहार्य है।
कानूनी विशेषज्ञों का मानना है कि मुख्य न्यायमूर्ति चंद्रशेखर के खिलाफ लगे आरोप
इसी गंभीर श्रेणी के हैं, और इसलिए न्याय मंत्रालय, सीबीआई तथा सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ द्वारा संयुक्त जांच और कठोर अनुशासनात्मक एवं आपराधिक कार्रवाई अनिवार्य है।
सुप्रीम कोर्ट ने यह स्पष्ट किया है कि जब कोई न्यायाधीश न्यायिक अधिकारों का दुरुपयोग करता है, संवैधानिक शपथ का उल्लंघन करता है या जनता के न्यायपालिका पर विश्वास को कमजोर करता है, तो उस पर कार्रवाई अनिवार्य है — ताकि न्यायपालिका की प्रतिष्ठा और पारदर्शिता बनी रहे। इनमें से प्रमुख मामले इस प्रकार हैं :
[Re C S Karnan (2017) 7 SCC 1, In Re. M.P. Dwivedi (1996) 4 SCC 152, Superintendent of Central Excise Vs. Somabhai Ranchhodhbhai Patel (2001) 5 SCC 65, Prabha Sharma Vs Sunil Goyal (2017) 11 SCC 77, R.R. Parekh v. High Court of Gujarat, (2016) 14 SCC 1, Muzaffar Husain v. State of U.P., 2022 SCC OnLine SC 567, Harish Arora v. Registrar of Coop. Societies, 2025 SCC OnLine Bom 2833, Mohd. Nazer M.P. v. State (UT of Lakshadweep), 2022 SCC OnLine Ker 7434, Prominent Hotels Vs. New Delhi Municipal Corporation 2015 SCC OnLine Del 11910]
इन सभी मामलों ने यह सिद्ध किया कि —
“न्यायपालिका अपनी मर्यादा, ईमानदारी और संवैधानिक जिम्मेदारी की रक्षा के लिए किसी भी स्तर पर समझौता नहीं कर सकती।”
कानून में निर्धारित प्रमुख धाराएँ और प्रावधान :
1. भारतीय संविधान का अनुच्छेद :- न्यायाधीशों पर अनुशासनात्मक कार्रवाई, निलंबन और विभागीय जांच करने का अधिकार प्रदान करता है। यह अनुच्छेद न्यायपालिका की आंतरिक जवाबदेही और नियंत्रण सुनिश्चित करता है।
2. Contempt of Courts Act, 1971 —धारा 2(बी) और धारा 12 के अनुसार,
यदि कोई न्यायाधीश जानबूझकर सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय के आदेशों की अवहेलना करता है, तो उस पर न्यायालय की अवमानना (Civil या Criminal Contempt) की कार्रवाई की जा सकती है। यह प्रावधान न्यायिक अनुशासन और संविधानिक व्यवस्था बनाए रखने के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है।
3. Prevention of Corruption Act, 1988 —धारा 13 के अंतर्गत, यदि कोई न्यायिक अधिकारी अपने पद का दुरुपयोग कर अनुचित लाभ प्राप्त करता है
या किसी अन्य को लाभ पहुँचाता है, तो यह गंभीर आपराधिक अपराध (Criminal Misconduct) माना जाता है। इस अधिनियम के तहत ऐसे न्यायाधीशों पर सीबीआई या अन्य जांच एजेंसियों द्वारा अभियोजन चलाया जा सकता है।
4. भारतीय न्याय संहिता (BNS) 2023 की धाराएँ 220, 221 और 222 —
यदि कोई सार्वजनिक अधिकारी (जिसमें न्यायाधीश भी शामिल हैं)
अवैध गिरफ्तारी करता है, जानबूझकर गलत आदेश पारित करता है, या कानून का उल्लंघन करता है, तो उसके खिलाफ फौजदारी मुकदमे (Criminal Prosecution) की स्पष्ट कानूनी व्यवस्था है।
इन सभी प्रावधानों का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि न्यायिक पद का दुरुपयोग, भ्रष्टाचार या संविधान-विरोधी आचरण करने वाला कोई भी न्यायाधीश कानून से ऊपर नहीं रह सकता।